मनुष्य अपनेमें कमीका अनुभव करता है तो दूसरोंका सहारा लेता है। जबतक यह परमात्माका आश्रय नहीं लेगा, तबतक उसकी कमी दूर नहीं होगी और वह दुःख पाता ही रहेगा। जीव परमात्माका ही अंश है, इसलिये परमात्माका सहारा लेनेसे ही उसकी कमी दूर होगी। द्वैत, अद्वैत आदि सभी उसका सहारा लेनेके लिये ही हैं। अद्वैत केवल द्वैतका निषेध करनेके लिये है। सभी मार्गोंमें त्याग मुख्य है; क्योंकि संसारसे माना हुआ सम्बन्ध ही बाँधनेवाला है।
साधन दो हैं- संसारसे सम्बन्ध तोड़ना और परमात्मासे सम्बन्ध जोड़ना। भगवान्के शरण होनेपर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद भगवान् करा देते हैं और जल्दी करा देते हैं-
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ।।
(गीता १२।७)
‘हे पार्थ! मुझमें आविष्ट चित्तवाले उन भक्तोंका मैं मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेवाला बन जाता हूँ।’
गुरु तो छोटा (चेला) बनाता है, पर भगवान् ऊँचा बनाते हैं। ऊँचे गुरु ऊँचा ही बनाते हैं। इसलिये दास्यरति सख्यरतिमें बदल जाती है। शरणमें जानेसे भगवान् अपने-आपको देते हैं। बालक माँका आश्रय लेता है तो माँ उसके वशमें हो जाती है। ‘हे नाथ! मैं आपका हूँ, और किसीका नहीं’- इसके आगे भगवान् निर्बल हो जाते हैं ! परन्तु जीवकी निर्बलता है-अन्यका सहारा लेना। अनन्यभक्तके लिये भगवान् सुलभ हैं-‘तस्याहं सुलभः पार्थ’ (गीता ८।१४) । भजनका भी आश्रय न मानकर केवल भगवान्के आश्रित हो जाय। यह शरणागतिका मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सुगम है। भगवान् भी शरणागत भक्तके शरण हो जाते हैं- ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्’ (गीता ४।११)।
दास्य, सख्य आदि भाव तत्त्वज्ञान होनेके बाद केवल चिन्मय तत्त्वमें ही होते हैं।
पूज्य स्वामी रामसुखदासजी
25119825









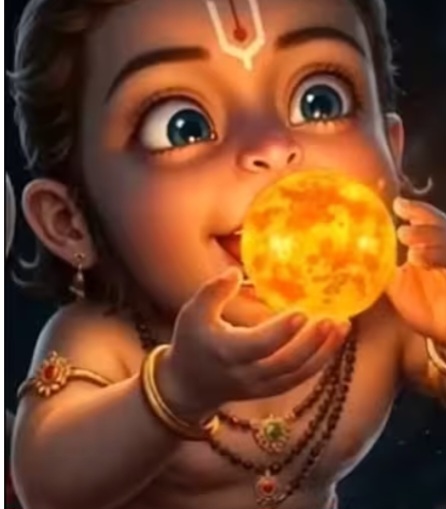
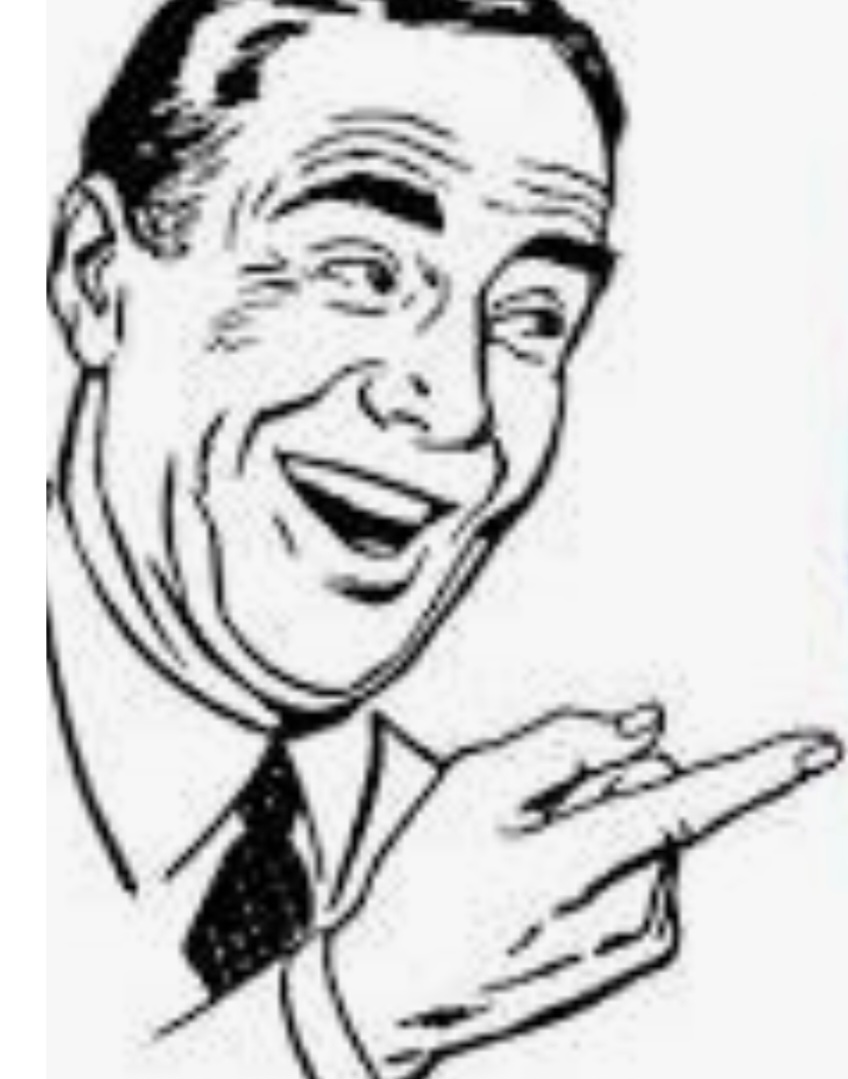





Leave a Reply